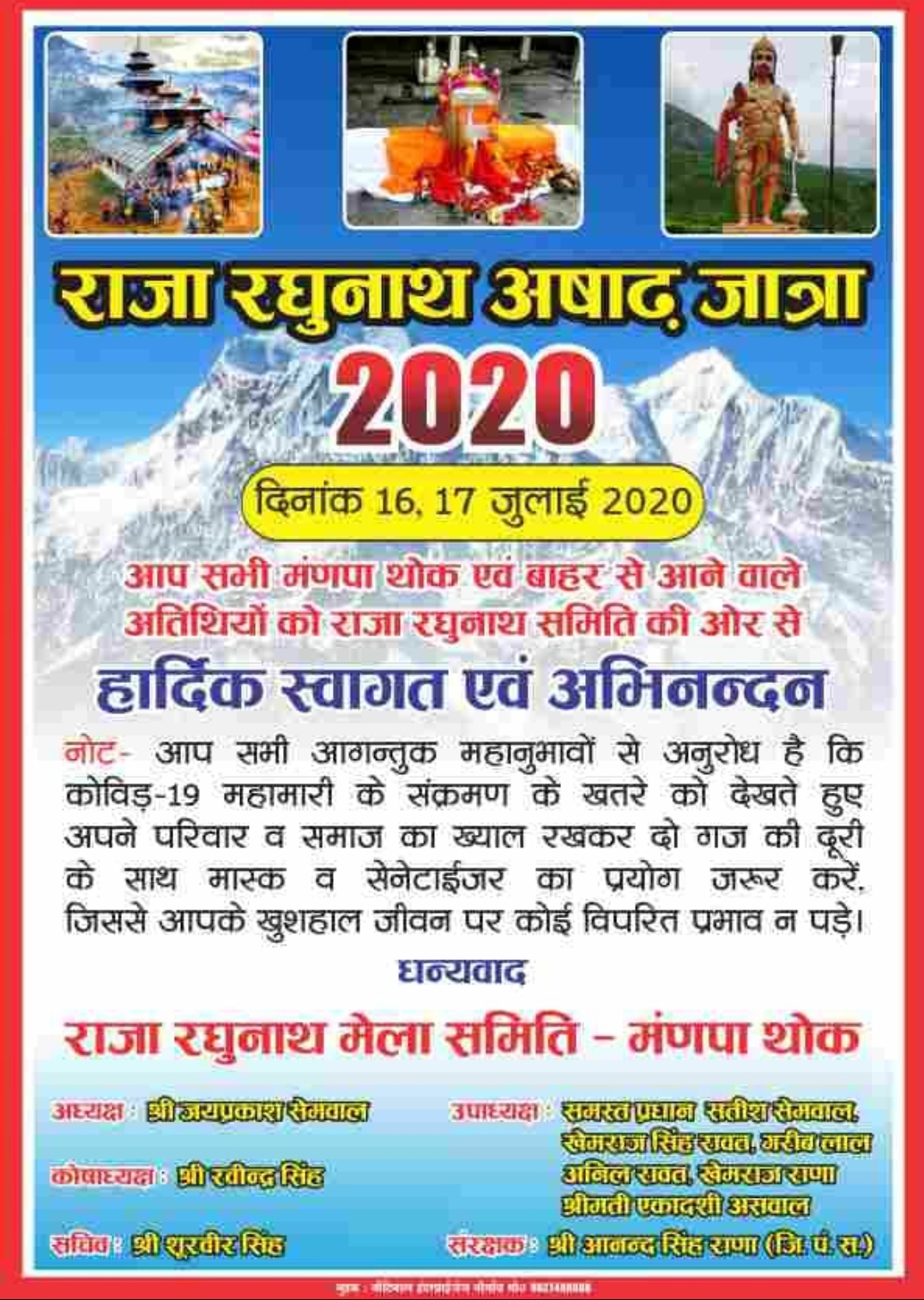मकर संक्रान्ति,लोहड़ी व पोंगल की नामो से जना जाता त्योहार
राजा भगीरथ सूर्यवंशी , तप साधना से गंगा को पृथ्वी अवतरित करवाया।।
उत्तरकाशी। 14-15 जनवरी का दिन उत्तर भारत में मकर संक्रान्ति के नाम से मनाया जाता है जिसका महत्व सूर्य के मकर रेखा की तरफ़ प्रस्थान करने को लेकर है कुंमाऊ उत्तरायण कहते हैं, पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पोंगल का त्यौहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का स्वागत कुछ अलग ही अंदाज में किया जाता है।सूर्य को अन्न-धन का दाता मानकर चार दिनों तक यह उत्सव मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आद्यशक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है, जो तन-मन-आत्मा को शक्ति प्रदान करता है।
संत-महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है। संकल्प शक्ति बढ़ती है। ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारत वर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है।
विष्णु धर्मसूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्व स्वास्थ्यवर्द्धन तथा सर्वकल्याण के लिए तिल के छः प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं- तिल जल से स्नान करना, तिल दान करना, तिल से बना भोजन, जल में तिल अर्पण, तिल से आहुति, तिल का उबटन लगाना।
सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्यकाल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा-अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धिकाल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए।
*रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। रामचरित मानस में ही भगवान श्री राम द्वारा पतंग उड़ाए जाने का भी उल्लेख मिलता है। मकर संक्रांति का जिक्र वाल्मिकी रचित रामायण में मिलता है।
राजा भगीरथ सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भगीरथ तप साधना के परिणामस्वरूप पापनाशिनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगाजल, अक्षत, तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है।
कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था, वह मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भगीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, ‘मातु गंगे त्रिकाल तक जन-जन का पापहरण करेंगी और भक्तजनों की सात पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेंगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेगा।’
महाभारत में पितामहा भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है।
सूर्य की सातवीं किरण भारत वर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। सातवीं किरण का प्रभाव भारत वर्ष में गंगा-जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या पूर्ण कुंभ तथा अर्द्धकुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन होता है।